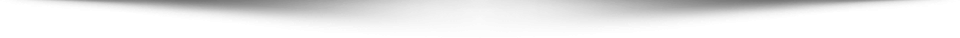ढाका । पाकिस्तानी गायक आतिफ असलम का 13 दिसंबर को ढाका में होने वाला कॉन्सर्ट रद्द हो गया है। आतिफ असलम ने अपने फेसबुक पोस्ट में बताया कि आयोजक फेल हो गए। उन्होंने कहा कि आयोजक बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से आवश्यक स्थानीय अनुमति, सुरक्षा मंजूरी और लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था नहीं करा पाए, इसलिए यह कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा।
यह कॉन्सर्ट बांग्लादेश के लिए विशेष रूप से संवेदनशील महीने दिसंबर में होना था, जब पूरा देश 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाता है। यह दिन 1971 के मुक्ति संग्राम की याद दिलाता है, जब नौ महीने के खूनी युद्ध के बाद पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया था और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा था। पाकिस्तानी कलाकार का इसी माह ढाका में प्रस्तुति देना कई लोगों को नागवार गुजरा था, जिसके बाद सुरक्षा चिंताएं भी सामने आई थीं। इसी दिन 93 हजार से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था।
आतिफ असलम ने अपने पोस्ट में लिखा- हमें यह दुख के साथ घोषणा करनी पड़ रही है कि 13 दिसंबर 2025 को ढाका में निर्धारित कॉन्सर्ट में हम प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। प्रमोटर्स और मैनेजमेंट आवश्यक स्थानीय अनुमतियां, सुरक्षा क्लीयरेंस और लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था नहीं कर सके।
बता दें कि ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब भारत-बांग्लादेश संबंधों में 2024 के बाद आई तल्खी के बीच पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ लोगों-से-लोगों के रिश्ते मजबूत करने की सक्रिय कोशिशें तेज कर दी हैं। इसके तहत पाकिस्तानी कलाकारों, खिलाड़ियों और सांस्कृतिक दल के ढाका दौरे बढ़ रहे हैं, दोनों देशों के बीच छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, सोशल मीडिया पर पाक-बांग्ला भाईचारा अभियान चलाया जा रहा है और इस्लामी एकजुटता के नाम पर युवा सम्मेलनों का आयोजन हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान इस मौके का इस्तेमाल दक्षिण एशिया में भारत के प्रभाव को कम करने और बांग्लादेश के भीतर अपने सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए कर रहा है।
विजय दिवस पर भव्य आयोजन
इस बीच बांग्लादेश 16 दिसंबर को अपना 54वां विजय दिवस धूमधाम से मना रहा है। इस अवसर पर दुनिया का सबसे बड़ा फ्लैग पैराशूटिंग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ढाका के तेजगांव पुराने हवाई अड्डे पर सुबह 11 बजे से बांग्लादेश थल सेना, नौसेना और वायु सेना अलग-अलग फ्लाई-पास्ट करेंगी। सुबह 11:40 बजे से टीम बांग्लादेश के 54 पैराट्रूपर्स हाथों में झंडे लेकर पैराशूट से उतरेंगे। इसके अलावा विशेष विजय दिवस बैंड शो का भी आयोजन होगा।
फरवरी 2026 में आम चुनाव
राजनीतिक मोर्चे पर भी बांग्लादेश में बड़े बदलाव की तैयारी है। अगस्त 2024 में छात्र-नेतृत्व वाले आंदोलन के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद से नोबेल विजेता प्रोफेसर मुहम्मद युनूस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार देश चला रही है।
अब 12 फरवरी 2026 को देश में आम चुनाव होने जा रहे हैं। इसी दिन जुलाई चार्टर पर राष्ट्रीय जनमत संग्रह भी होगा, जिसमें कार्यकारी शक्ति पर अंकुश, न्यायपालिका की स्वतंत्रता मजबूत करने समेत कई बड़े संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव है। 300 संसदीय सीटों के लिए एक साथ मतदान होगा। यह चुनाव और जनमत संग्रह बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है।