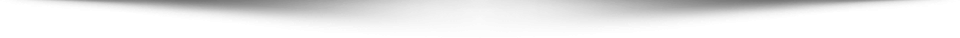नई दिल्ली। भारत (India) में आयकर विभाग (Income Tax Department) ने सभी टैक्सपेयर के लिए PAN और Aadhaar लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। अगर दोनों दस्तावेज़ लिंक नहीं हैं, तो आपका PAN “इनएक्टिव” माना जा सकता है, जिससे वित्तीय लेनदेन, टैक्स रिफंड, बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन और निवेश संबंधी काम रुक सकते हैं। बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि उनका PAN-Aadhaar लिंक हुआ है या नहीं, लेकिन हर बार वेबसाइट पर जाकर चेक करना झंझट भरा लगता है।
SMS भेजकर करें चेक
अब सरकार ने इसका बेहद आसान तरीका पेश किया है SMS के जरिए PAN-Aadhaar लिंक स्टेटस चेक करने की सुविधा। इसका मतलब है कि अब आपको इंटरनेट या वेबसाइट की जरूरत नहीं, बस एक छोटा-सा संदेश भेजकर आप पता लगा सकते हैं कि आपका PAN और Aadhaar लिंक है या नहीं। यह तरीका खासकर ग्रामीण इलाकों या कम इंटरनेट वाले क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। आइए जानते हैं कि कैसे आप एक साधारण SMS भेजकर अपना PAN-Aadhaar लिंक स्टेटस मिनटों में जान सकते हैं, और अगर लिंक न हो तो क्या करें।
SMS से PAN-Aadhaar लिंक स्टेटस कैसे चेक करें
अब आप बिना वेबसाइट खोले या इंटरनेट इस्तेमाल किए, सिर्फ एक SMS भेजकर PAN-Aadhaar लिंक स्टेटस जान सकते हैं। इसके लिए नीचे बताए गए स्टेप्स फॉलो करें: अगली स्लाइड में जानिये स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस:
Step 1:
अपने मोबाइल फोन का SMS ऐप खोलें। अब एक नया मैसेज टाइप करें इस फॉर्मेट में 👉 UIDPAN <स्पेस> <12 अंकों का Aadhaar नंबर> <स्पेस> <10 अंकों का PAN नंबर> उदाहरण: UIDPAN 123456789012 ABCDE1234F
Step 2:
यह मैसेज 567678 या 56161 नंबर पर भेजें। कुछ ही सेकंड में आपको आयकर विभाग की ओर से एक SMS रिप्लाई मिलेगा जिसमें लिखा होगा कि आपका PAN और Aadhaar “Linked” है या “Not Linked”। अगर आपका PAN-Aadhaar लिंक हो चुका है, तो आपको मिलेगा: “Your PAN <PAN Number> is already linked with Aadhaar <Aadhaar Number>.” अगर लिंक नहीं हुआ है, तो मैसेज मिलेगा: “Your PAN <PAN Number> is not linked with Aadhaar <Aadhaar Number>.”
अगर PAN और Aadhaar लिंक नहीं है, तो क्या करें?
अगर SMS के जरिए पता चलता है कि आपका PAN और Aadhaar लिंक नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप नीचे दिए गए किसी भी तरीके से इसे लिंक कर सकते हैं: तरीका 1: ऑनलाइन वेबसाइट से https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं। “Link Aadhaar” सेक्शन खोलें। PAN, Aadhaar नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें। OTP के जरिए वेरिफिकेशन करें और लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करें।
तरीका 2:
SMS के जरिए लिंक करें। आप SMS के जरिए भी PAN-Aadhaar लिंक कर सकते हैं फॉर्मेट वही रहेगा: UIDPAN <12-digit Aadhaar> <10-digit PAN>और इसे 567678 या 56161 पर भेजें।
अगर PAN-Aadhaar लिंक नहीं है तो क्या नुकसान हो सकता है?
आपका PAN नंबर इनएक्टिव हो जाएगा। आप ITR (Income Tax Return) फाइल नहीं कर पाएंगे। बैंक और म्यूचुअल फंड जैसे वित्तीय लेनदेन रुक सकते हैं। आपका क्रेडिट स्कोर प्रभावित हो सकता है। सरकारी सब्सिडी और PF से जुड़ी सेवाओं में दिक्कत आ सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि आप जल्द से जल्द लिंकिंग की स्थिति जांचें और जरूरत हो तो इसे तुरंत लिंक करें।